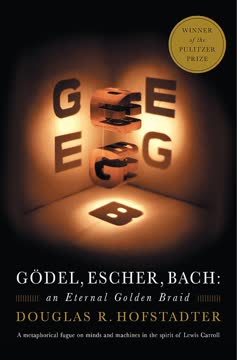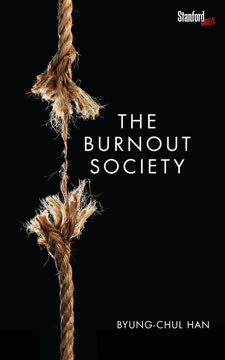मुख्य निष्कर्ष
1. बुद्धिमत्ता जैविक अनुकूलन का सर्वोच्च रूप है, जो आत्मसात और अनुकूलन के बीच संतुलन बनाती है।
बुद्धिमत्ता को उन गतिशील संरचनाओं की प्रगतिशील पुनरावृत्ति के रूप में परिभाषित करना, जो यह बनाती है, इस बात को दोहराने के समान है कि बुद्धिमत्ता वह संतुलन की स्थिति है जिसकी ओर संवेदी-चालक और संज्ञानात्मक प्रकृति के सभी क्रमिक अनुकूलन तथा जीव और पर्यावरण के बीच सभी आत्मसात और अनुकूलनात्मक अंतःक्रियाएँ अग्रसर होती हैं।
अनुकूलन ही मुख्य है। बुद्धिमत्ता कोई अलग क्षमता नहीं, बल्कि अनुकूलन का सबसे उन्नत रूप है, जो जीव के पर्यावरण पर क्रिया (आत्मसात) और पर्यावरण के जीव पर प्रभाव (अनुकूलन) के बीच संतुलन स्थापित करती है। आत्मसात का अर्थ है वास्तविकता को मौजूदा मानसिक संरचनाओं या "स्कीमाओं" में समाहित करना, जबकि अनुकूलन का अर्थ है उन संरचनाओं को नई वास्तविकता के अनुरूप संशोधित करना।
कार्यात्मक निरंतरता। यह अनुकूलनात्मक दृष्टिकोण बुद्धिमत्ता को सभी जैविक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के साथ एक सतत प्रवाह में रखता है, जो सरल रिफ्लेक्स और धारणा से लेकर जटिल तर्क तक फैली होती हैं। यह इन प्रक्रियाओं के लिए अंतिम संतुलन की स्थिति है, जो अपनी लचीलेपन और स्थायित्व से पहचानी जाती है। बुद्धिमत्ता पर्यावरण के साथ स्थान और समय में बढ़ती दूरी पर संवाद संभव बनाती है, जिससे क्रिया तत्काल "यहाँ और अब" से मुक्त हो जाती है।
संतुलन की प्राप्ति। आत्मसात और अनुकूलन के बीच संतुलन बुद्धिमत्ता के विकास के साथ अधिक गतिशील और स्थिर होता जाता है। यह गतिशील संतुलन, जो पुनरावृत्तीय क्रियाओं में परिणत होता है, व्यक्ति को लचीले और शक्तिशाली ढंग से दुनिया को समझने और उसके साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिससे अनुकूलन प्रक्रियाएँ व्यापक वास्तविकता तक फैलती हैं।
2. बुद्धिमत्ता मौलिक रूप से क्रियात्मक है, जो आंतरिकीकृत, पुनरावृत्तीय क्रियाओं से बनी संरचित प्रणालियाँ बनाती है जिन्हें समूह कहा जाता है।
क्रियाओं की विशिष्ट प्रकृति, अनुभवजन्य क्रियाओं की तुलना में, इस तथ्य पर निर्भर करती है कि वे कभी भी असतत अवस्था में नहीं होतीं।
क्रियाएँ ही क्रियाएँ हैं। तार्किक और गणितीय सोच केवल बाहरी विचारों को समझना नहीं है, बल्कि "क्रियाओं" से बनी है, जो आंतरिकीकृत क्रियाएँ हैं। ये अलग-थलग क्रियाएँ नहीं, बल्कि संगठित प्रणालियाँ हैं, जो सरल अनुभवजन्य क्रियाओं या सहज प्रतिनिधित्वों से भिन्न हैं।
प्रणालियाँ समूह हैं। इन क्रियात्मक प्रणालियों को "समूह" कहा जाता है, जिनकी विशिष्ट विशेषताएँ हैं:
- संयोजनशीलता: क्रियाओं को जोड़ा जा सकता है।
- पुनरावृत्तीयता: हर क्रिया का एक विपरीत होता है जो उसे उलट सकता है।
- संघटनशीलता: परिणाम तक पहुँचने का मार्ग परिणाम को नहीं बदलता।
- पहचान: एक क्रिया और उसका विपरीत मिलकर शून्य हो जाते हैं।
- स्वयंसिद्धता (गुणात्मक समूहों के लिए): क्रिया को दोहराने से परिणाम नहीं बदलता (A+A=A)।
जीवित तर्क। समूह सोच के संतुलन की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गतिशीलता और स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये औपचारिक तर्क के मनोवैज्ञानिक आधार हैं, जिसे इस संतुलन का स्वयंसिद्ध मॉडल माना जाता है, न कि मन पर थोपे गए पूर्वनिर्धारित ढांचे के रूप में।
3. धारणा बुद्धिमत्ता से अपनी अपरिवर्तनीय, सांख्यिकीय प्रकृति के कारण भिन्न होती है, जबकि बुद्धिमत्ता गतिशील, पुनरावृत्तीय क्रियाओं के माध्यम से वस्तुनिष्ठ सापेक्षता प्राप्त करती है।
एक धारणा संरचना, जैसा कि गेस्टाल्ट सिद्धांत स्वयं जोर देता है, इसे योगात्मक संयोजन में अपूरणीयता द्वारा पहचाना जाता है—इसलिए यह अपरिवर्तनीय और गैर-संघटनशील होती है।
धारणा की सीमाएँ। गेस्टाल्ट सिद्धांत धारणा संरचनाओं की "समग्र" प्रकृति को उजागर करता है, पर ये संरचनाएँ क्रियात्मक समूहों से मौलिक रूप से भिन्न होती हैं। धारणा की विशेषताएँ हैं:
- अपरिवर्तनीयता: धारणा में परिवर्तन अक्सर बिना क्षतिपूर्ति के होते हैं।
- गैर-योगात्मकता: समग्र भागों का सरल योग नहीं होता।
- गैर-संघटनशीलता: धारणा मार्ग पर निर्भर करती है।
- विकृत सापेक्षता: धारणा भेदों को बढ़ा देती है (वेबर का नियम) और भ्रमों की शिकार होती है।
सांख्यिकीय प्रकृति। धारणा तंत्र संभावनाओं और ध्यान के सांख्यिकीय वितरण पर आधारित होते हैं, जिससे "अक्षतिपूर्ति परिवर्तन" और "संतुलन के विस्थापन" होते हैं, जो क्रियात्मक सोच की सटीक क्षतिपूर्ति और स्थायी संतुलन से भिन्न हैं।
क्रियात्मक वस्तुनिष्ठता। बुद्धिमत्ता अपनी गतिशील और पुनरावृत्तीय क्रियाओं के माध्यम से एक भिन्न प्रकार की सापेक्षता—वस्तुनिष्ठ सापेक्षता—प्राप्त करती है। यह कई दृष्टिकोणों का समन्वय और परिवर्तन की क्षतिपूर्ति करके धारणा की विकृतियों को पार कर स्थिर अवधारणाएँ जैसे संरक्षण प्रदान करती है।
4. आदत और संवेदी-चालक बुद्धिमत्ता की उत्पत्ति संवेदी-चालक आत्मसात में समान है, पर बुद्धिमत्ता तत्काल, कठोर प्रतिक्रियाओं से परे विस्तारित होती है।
आदत और बुद्धिमत्ता के बीच निकटता स्पष्ट हो जाती है, दोनों, यद्यपि विभिन्न स्तरों पर, संवेदी-चालक आत्मसात से उत्पन्न होते हैं।
साझा आधार। आदत निर्माण और बुद्धिमत्ता की शुरुआत दोनों संवेदी-चालक आत्मसात से होती हैं, जो नए अनुभवों को मौजूदा क्रिया स्कीमाओं में समाहित करने की प्रक्रिया है। सरल सशर्त प्रतिक्रियाएँ भी केवल निष्क्रिय संघ नहीं, बल्कि पूर्व-स्थित व्यवहार पैटर्न में नए तत्वों को जोड़ना हैं।
कठोरता से परे। जहाँ आदतें पुनरावृत्त, एकतरफा प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती हैं, बुद्धिमत्ता तब उभरती है जब यह आत्मसात गतिविधि तत्काल, कठोर संबंधों से आगे बढ़ती है। इसमें शामिल हैं:
- बढ़ी हुई गतिशीलता: स्कीमाएँ अधिक लचीली हो जाती हैं और नए तरीकों से संयोजित की जा सकती हैं।
- विस्तारित दायरा: क्रिया तत्काल वर्तमान से परे घटनाओं की पूर्वधारणा और पुनर्निर्माण करती है।
- साधन और उद्देश्य का विभाजन: लक्ष्य पहले निर्धारित होते हैं, फिर साधन लागू होते हैं।
गतिविधि की निरंतरता। प्रयास-और-त्रुटि, जिसे अक्सर आदत और प्रारंभिक बुद्धिमत्ता का आधार माना जाता है, पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं है, बल्कि मौजूदा स्कीमाओं और अर्थों द्वारा निर्देशित होती है। यह सक्रिय अनुकूलन, आत्मसात के साथ मिलकर, सरल आदतों से जटिल बुद्धिमान व्यवहारों के विकास को प्रेरित करता है।
5. संवेदी-चालक बुद्धिमत्ता जटिल क्रिया स्कीमाओं के चरणों से विकसित होती है, जो व्यावहारिक वस्तु स्थिरता और स्थानिक समूहों में परिणत होती है।
प्रारंभिक बुद्धिमत्ता केवल गतिशील संतुलन का वह रूप है जिसकी ओर धारणा और आदत के अनुकूलन तंत्र अग्रसर होते हैं; परन्तु ये तब तक इसे प्राप्त नहीं करते जब तक वे अपने-अपने क्षेत्र छोड़ते नहीं।
पूर्व-भाषाई आधार। भाषा से पहले, बुद्धिमत्ता छह चरणों में संवेदी-चालक समन्वय के माध्यम से विकसित होती है। शिशु रिफ्लेक्स और प्राथमिक आदतों से शुरू होकर:
- प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (शरीर-केंद्रित पुनरावृत्ति)
- द्वितीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (बाहरी वस्तुओं पर क्रिया)
- द्वितीयक स्कीमाओं का समन्वय (साधन-उद्देश्य व्यवहार)
- तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (सक्रिय प्रयोग)
- मानसिक संयोजन के माध्यम से आविष्कार (आंतरिकीकृत क्रिया)
वस्तु और स्थान निर्माण। यह विकास मौलिक अवधारणाओं जैसे वस्तु स्थिरता और स्थानिक संबंधों के निर्माण से गहराई से जुड़ा है। वस्तु स्थिरता, अर्थात वस्तुएँ न देखे जाने पर भी मौजूद रहती हैं, संवेदी-चालक स्कीमाओं के समन्वय से धीरे-धीरे उभरती है, विशेषकर खोज और विस्थापन से संबंधित।
व्यावहारिक समूह। इस अवधि के अंत तक (लगभग 1.5-2 वर्ष), बच्चा एक व्यावहारिक "विस्थापन समूह" बनाता है। यह स्थानिक परिवर्तनों (गति, उलट, चक्कर) और स्थिति संरक्षण की अनुभवजन्य समझ है, जो शारीरिक क्रियाओं के समन्वय से प्राप्त होती है, न कि वैचारिक सोच से।
6. सोच पूर्व-क्रियात्मक चरणों (प्रतीकात्मक, पूर्व-सैद्धांतिक, सहज) के माध्यम से विकसित होती है, जो स्वकेंद्रितता, अनुभववाद और अपरिवर्तनीय मानसिक प्रयोगों से चिह्नित हैं।
सहज सोच हमेशा विकृत स्वकेंद्रितता प्रदर्शित करती है, क्योंकि मान्यता प्राप्त संबंध विषय की क्रिया से जुड़ा होता है, न कि वस्तुनिष्ठ प्रणाली में विकेंद्रीकृत।
प्रतीकात्मक कार्य। संवेदी-चालक बुद्धिमत्ता से सोच का संक्रमण प्रतीकात्मक कार्य के उदय से होता है (लगभग 1.5-2 वर्ष), जो प्रतीकों, संकेतों के माध्यम से प्रतिनिधित्व संभव बनाता है। इसमें विलंबित अनुकरण, प्रतीकात्मक खेल, मानसिक चित्रण और भाषा अधिग्रहण शामिल हैं।
पूर्व-सैद्धांतिक सोच। पहला चरण (लगभग 2-4 वर्ष) "पूर्व-सैद्धांतिक" होता है, जो "पूर्व-धारणाओं" का उपयोग करता है, जो व्यक्तिगत उदाहरणों और सामान्य वर्गों के बीच मध्यवर्ती होते हैं। तर्क "स्थानांतरणीय" होता है, जो तत्काल समानताओं या कल्पित क्रियाओं के आधार पर विशेष से विशेष तक जाता है, बिना तार्किक संरचना और पुनरावृत्ति के।
सहज सोच। अगला चरण (लगभग 4-7 वर्ष) "सहज" होता है, जिसमें मानसिक प्रतिनिधित्व धारणा विन्यासों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। सोच अभी भी:
- स्वकेंद्रित: विषय के दृष्टिकोण पर केंद्रित, विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय नहीं करता।
- अनुभववादी: तत्काल दृश्य पर केंद्रित, गहन वास्तविकता पर नहीं।
- अपरिवर्तनीय: मानसिक परिवर्तन एकतरफा होते हैं।
नियम, न कि क्रियाएँ। सहज सोच "व्यवस्थित सहजता" के माध्यम से प्रगति करता है, जहाँ नियम (धारणा समायोजनों के समान) विकृतियों को सुधारते हैं और अधिक सटीक प्रतिनिधित्व लाते हैं। फिर भी ये पूर्ण पुनरावृत्तीय क्रियाएँ नहीं हैं और सच्चे तर्क की संयोजक संरचना से वंचित हैं।
7. ठोस क्रियात्मक सोच पुनरावृत्तीय समूहों के निर्माण के साथ उभरती है, जो संरक्षण और तार्किक तर्क को संभव बनाती है जो संचालित वस्तुओं से जुड़ी होती है।
जहाँ "समूह" होता है, वहाँ समग्र का संरक्षण होगा, और यह संरक्षण केवल संभावित अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि सोच में निश्चितता के रूप में स्थापित होगा।
क्रियात्मक परिवर्तन। लगभग 7-8 वर्ष की आयु में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है: सहज नियम पुनरावृत्तीय क्रियाओं में बदल जाते हैं, जो "ठोस समूह" बनाते हैं। यह परिवर्तन अक्सर तीव्र होता है और बच्चे की संरक्षण के प्रति निश्चितता से पहचाना जाता है।
संरक्षण की पहचान। क्रियात्मक सोच का मुख्य संकेत संरक्षण की समझ है—कि मात्रा रूपांतरणों के बावजूद समान रहती है। यह लागू होता है:
- पदार्थ (लगभग 7-8 वर्ष)
- भार (लगभग 9-10 वर्ष)
- आयतन (लगभग 11-12 वर्ष)
ठोस तर्क। ये क्रियाएँ "ठोस" हैं क्योंकि वे उन वस्तुओं से जुड़ी हैं जिन्हें संचालित या सीधे देखा जा सकता है। ये वर्गीकरण, संबंध (क्रमबद्धता), संख्याओं, और स्थान-काल अवधारणाओं जैसे मापन और समय पर तार्किक तर्क सक्षम करती हैं। हालांकि, यह तर्क अभी सामान्यीकृत नहीं है और एक प्रकार की सामग्री (जैसे पदार्थ) पर पहले लागू हो सकता है, फिर दूसरे (जैसे भार) पर।
8. औपचारिक क्रियात्मक सोच, किशोरावस्था में प्रकट होती है, जो क्रियाओं पर क्रियाएँ संचालित करती है, जिससे संभाव्य-निष्कर्षात्मक तर्क संभव होता है जो ठोस वास्तविकता से स्वतंत्र होता है।
औपचारिक सोच का अर्थ है इन क्रियाओं पर चिंतन करना और इसलिए क्रियाओं या उनके परिणामों पर क्रिया करना, जिससे क्रियाओं का द्वितीयक समूह बनता है।
सोच पर सोच। लगभग 11-12 वर्ष की आयु से किशोर "औपचारिक क्रियाएँ" विकसित करते हैं। इसमें केवल ठोस वस्तुओं और उनके रूपांतरणों के बारे में नहीं, बल्कि स्वयं क्रियाओं के बारे में सोच शामिल है। यह सोच का "द्वितीयक स्तर" है।
संभाव्य-निष्कर्षात्मक तर्क। औपचारिक सोच सक्षम बनाता है:
- अनुमानों से तर्क: ऐसी संभावनाओं पर विचार करना जो वास्तविक न भी हों।
- रूप के आधार पर निष्कर्ष: तर्क के तार्किक ढांचे के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सामग्री से स्वतंत्र।
- प्रस्तावों का संचालन: कथनों और उनके तार्किक संबंधों (निहितार्थ, विरोधाभास) पर तर्क करना।
सार और सामान्य। यह चरण समस्या के सभी संभावित समाधानों का व्यवस्थित और सारगर्भित अन्वेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। यह वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच की नींव है, जो बुद्धिमत्ता को तत्काल वास्तविकता से परे संभावित की दुनिया तक विस्तारित करता है।
9. बौद्धिक विकास लगातार निर्माणों की एक श्रेणी है, जहाँ प्रत्येक स्तर पिछले स्तर की संरचनाओं का समन्वय और विभेदन करता है।
इन स्तरों में से प्रत्येक से अगले स्तर में संक्रमण नए समन्वय और पिछले स्तर की इकाई बनाने वाली प्रणालियों के विभेदन दोनों द्वारा चिह्नित होता है।
निर्माण खंड। विकास एक सहज, निरंतर संचय नहीं, बल्कि विशिष्ट चरणों की श्रृंखला है, जो प्रत्येक पिछले स्तर की संरचनाओं पर आधारित और उन्हें परिवर्तित करती है। उच्चतर स्तर की संरचनाएँ निचले स्तर के तत्वों के नए समन्वय हैं।
विभेदन। समन्वय के साथ-साथ विकास में विभेदन भी होता है। प्रारंभ में, विभिन्न कार्य (जैसे तार्किक, स्थानिक, व्यावहारिक तर्क) संवेदी-चालक स्कीमाओं में अविभाजित होते हैं। विकास के साथ, ये कार्य अलग-अलग क्रियात्मक प्रणालियों (जैसे तार्किक बनाम स्थान-काल समूह) में विभेदित होते हैं।
प्रगतिशील संतुलन। प्रत्येक चरण पिछले की तुलना में अधिक स्थिर और गतिशील संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। संवेदी-चालक बुद्धिमत्ता व्यावहारिक संतुलन प्राप्त करती है, सहज सोच अस्थिर होती है, ठोस क्रियाएँ ठोस समस्याओं के लिए स्थिर संतुलन प्राप्त करती हैं, और औपचारिक क्रियाएँ सार समस्याओं के लिए सामान्य संतुलन प्राप्त करती हैं।
10. सामाजिक अंतःक्रिया, विशेषकर सहयोग, तर्क के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दृष्टिकोणों के समन्वय और विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है।
सहयोग व्यवहार के उन प्रारंभिक रूपों में से पहला है जो तर्क की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सामाजिक प्रभाव। समाज भाषा (संकेत), साझा ज्ञान (मूल्य), और सामूहिक मानदंडों (तर्क) के माध्यम से बुद्धिमत्ता पर गहरा प्रभाव डालता है। हालांकि, इस प्रभाव की प्रकृति बच्चे के विकासात्मक चरण के अनुसार बदलती है।
पूर्व-क्रियात्मक स्वकेंद्रितता। पूर्व-क्रियात्मक अवधि में, बच्चे की स्वकेंद्रितता (अपना दृष्टिकोण दूसरों से अलग न कर पाना) उसे बाहरी सुझाव और बाधा के प्रति संवेदनशील बनाती है, परन्तु सच्चे बौद्धिक आदान-प्रदान में बाधा डालती है। वे सामाजिक इनपुट को अपने दृष्टिकोण में आत्मसात करते
अंतिम अपडेट:
समीक्षाएं
बुद्धिमत्ता का मनोविज्ञान को मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिली हैं, जहाँ कई लोग इसे संज्ञानात्मक विकास को समझने में महत्वपूर्ण मानते हैं। पाठक पियाजे के उन क्रांतिकारी सिद्धांतों की सराहना करते हैं, जो बताते हैं कि कैसे बुद्धिमत्ता शैशवावस्था से किशोरावस्था तक विकसित होती है। हालांकि, कुछ लोगों के लिए यह पुस्तक शैक्षणिक भाषा और जटिल अवधारणाओं के कारण चुनौतीपूर्ण साबित होती है। कई समीक्षक इसे मनोविज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए अनिवार्य पठन बताते हैं, जबकि कुछ इसके गहन विषयवस्तु से जूझते हैं। कठिनाइयों के बावजूद, कई पाठक पियाजे की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, अनुकूलन और विकास के चरणों पर दी गई अंतर्दृष्टि को मूल्यवान मानते हैं।
Similar Books