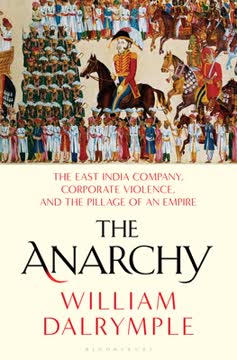मुख्य निष्कर्ष
1. अंबेडकर की जटिल विरासत: एक राष्ट्र के बदलते देवता
एक राष्ट्र अपने विचारों में, अपने पवित्र साहित्य में, लकड़ी और पत्थर में देवताओं का निर्माण करता है... जब राष्ट्र शारीरिक रूप से पराजित होता है, जब इसे आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से पराजित किया जाता है, तो इसे स्थानांतरित किया जाता है, और मजबूरी में यह वास्तव में उन प्रतिनिधित्वों को सार्वजनिक स्थानों से हटा कर निजी निवासों में स्थानांतरित कर देता है।
प्रतिनिधित्व का स्थानांतरण। राष्ट्र ऐसे देवताओं का निर्माण करते हैं जो उनके संचित अनुभवों और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। जब एक राष्ट्र पराजित होता है, तो यह अक्सर अपने स्वयं के देवताओं को छोड़ देता है और विजेताओं के देवताओं की पूजा करने लगता है। यह मूर्तिपूजा और अस्वीकृति का चक्र इतिहास में एक पुनरावृत्त विषय है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है।
आधुनिक मूर्तिपूजा। समकालीन भारत में, अंबेडकर जैसे व्यक्तियों को लगभग देवता के स्तर पर elevated किया गया है, उनके सम्मान में मूर्तियाँ, छुट्टियाँ और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यह देवत्व अन्य राष्ट्रीय नायकों की उपेक्षा और गांधी जैसे व्यक्तियों की आलोचना के साथ स्पष्ट रूप से विपरीत है।
इतिहास का उलटफेर। यह मूर्तिपूजा कई कारकों के संयोजन से प्रेरित है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम को पाठ्यपुस्तकों में कुछ पैरा तक सीमित करना, जातिवादी राजनीति का उदय, और अंबेडकर के कुछ अनुयायियों द्वारा इस्तेमाल किया गया मौखिक आतंकवाद शामिल है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहाँ देश के दुश्मनों के साथ सहयोग करने वाले व्यक्तियों को अब पूजा जाता है, जबकि स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों की अक्सर आलोचना की जाती है।
2. स्वतंत्रता सेनानी: अंबेडकर की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षा
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़े किसी भी गतिविधि में अंबेडकर ने भाग नहीं लिया, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है।
संघर्ष से अनुपस्थिति। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ सार्वजनिक करियर होने के बावजूद, अंबेडकर ने उस आंदोलन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया। इसके बजाय, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के अभियानों का लगातार विरोध किया और इसके विफलताओं पर खुशी मनाई।
ब्रिटिशों के प्रति वफादारी। अंबेडकर की रचनाएँ और क्रियाएँ ब्रिटिश शासकों के प्रति गहरी वफादारी को प्रकट करती हैं। उन्होंने उनसे अनुसूचित जातियों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को मान्यता देने की अपील की, यह तर्क करते हुए कि भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व अछूतों की मदद पर निर्भर था।
कांग्रेस का विरोध। अंबेडकर ने कांग्रेस और उसके नेताओं का सक्रिय रूप से विरोध किया, उनके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को "शासन करने वाली वर्गों" के अत्याचार को बनाए रखने के लिए एक धोखा समझते हुए। उन्होंने कांग्रेस को एक हिंदू संस्था और गांधी को एक पाखंडी के रूप में चित्रित किया जो अछूतों को धोखा दे रहा था।
3. वफादार मंत्री: ब्रिटिश सरकार में अंबेडकर की सेवा
इस प्रकार, जबकि वर्षों ने देश की स्वतंत्रता में culminate किया, अंबेडकर के मामले में यह उनके वायसराय की परिषद के सदस्य बनने में culminate हुआ, अर्थात्—वर्तमान शब्दों में—ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री।
ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री। जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था, अंबेडकर ने ब्रिटिश वायसराय की परिषद में मंत्री के रूप में एक पद स्वीकार किया। यह नियुक्ति उनके लंबे समय के ब्रिटिश सहयोग का परिणाम थी।
समन्वित क्रियाएँ। अंबेडकर की क्रियाएँ अक्सर ब्रिटिशों के साथ समन्वित होती थीं, जो उनके हितों की सेवा करती थीं और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करती थीं। उन्हें कांग्रेस के खिलाफ एक संतुलन के रूप में इस्तेमाल किया गया, और उनके विचारों को ब्रिटिशों द्वारा बढ़ावा दिया गया ताकि वे असहमति और विभाजन पैदा कर सकें।
कांग्रेस की निंदा। एक मंत्री के रूप में, अंबेडकर ने सक्रिय रूप से कांग्रेस और उसके नेताओं की निंदा की, ब्रिटिश कथा को दोहराते हुए कि कांग्रेस एक हिंदू संस्था थी और उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई एक धोखा थी। उन्होंने गांधी के आंदोलन को "अन्यायपूर्ण" और "अनावश्यक" बताया।
4. जिस सरकार में उन्होंने शामिल हुए: सहयोग और सुविधा का अध्ययन
दुर्भाग्यवश, वह अपनी स्थिति की कठिनाइयों को उन प्रभावों के काम के प्रति श्रेय देने के लिए प्रवृत्त हैं जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि वह अवसादित वर्गों के सदस्य हैं, और इससे यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि हम उनके बारे में अत्यधिक चिंतित नहीं हैं क्योंकि हम यह नहीं सोचते कि अवसादित वर्गों का समर्थन प्राप्त करना सार्थक है।
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। प्रभाव के एक पद की इच्छा अंबेडकर के ब्रिटिशों के साथ सहयोग का एक प्रेरक बल थी। उन्होंने अक्सर अपनी कठिनाइयों को भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्राथमिक चिंता अपनी उन्नति थी।
ब्रिटिश गणनाएँ। ब्रिटिशों ने अंबेडकर को कांग्रेस का मुकाबला करने और भारतीय समाज को विभाजित करने के अपने प्रयासों में एक उपयोगी सहयोगी के रूप में देखा। उन्होंने उन्हें प्रभाव के पदों से पुरस्कृत किया और उनके विचारों का उपयोग अपनी नीतियों को सही ठहराने के लिए किया।
सुविधाजनक गठबंधन। अंबेडकर का ब्रिटिशों के साथ सहयोग एक सुविधाजनक गठबंधन था जो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और ब्रिटिशों की विभाजन और शासन की रणनीति दोनों की सेवा करता था। वह ऐसे पदों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे जो ब्रिटिशों के लिए सुविधाजनक थे, भले ही वे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करते थे।
5. सामाजिक सुधारक: एक ब्रिटिश रणनीति और उसका भारतीय प्रवक्ता
भारत के लिए उन्नीसवीं सदी के अंतिम भाग और बीसवीं सदी के पहले भाग का एक बड़ा विषय है: राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आंदोलन के नेता... हमारे संस्कृति और धर्म के बारे में जो अपमानजनक बातें ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश शासकों ने हमारे मन में रोपित की थीं, उन्हें पलटने के लिए एक महान प्रयास में लगे हुए थे।
मिशनरी प्रभाव। ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश शासकों ने लंबे समय से भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने का प्रयास किया। अंबेडकर की रचनाएँ और क्रियाएँ अक्सर इन अपमानों को प्रतिध्वनित करती हैं, हिंदू समाज को स्वाभाविक रूप से दमनकारी और अन्यायपूर्ण के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
विभाजन और शासन। ब्रिटिशों ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभाजन और शासन की रणनीति का उपयोग किया। उन्होंने भारतीय समाज में विभाजन उत्पन्न करने का प्रयास किया, यह प्रचार करते हुए कि विभिन्न समूहों के पास असंगत हित हैं।
अंबेडकर की भूमिका। अंबेडकर इस रणनीति में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, अनुसूचित जातियों की अलगाव की वकालत करते हुए और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करते हुए। उनके विचार अक्सर ब्रिटिशों और मिशनरियों के विचारों के साथ मेल खाते थे।
6. क्या हम समय के मनु?: अंबेडकर की संवैधानिक भूमिका पर प्रश्न
कांग्रेस का संविधान सभा पर पूर्ण नियंत्रण था... यह कांग्रेस नेताओं की उदारता और उनके निर्णय के कारण था कि सभी को राष्ट्रीय कार्य को पूरा करने में शामिल होना चाहिए कि अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष 'चुना' गया।
लेखन का मिथक। व्यापक विश्वास के बावजूद कि अंबेडकर भारतीय संविधान के एकमात्र लेखक थे, वास्तविकता यह है कि वह कई योगदानकर्ताओं में से एक थे। संविधान एक सामूहिक प्रयास का परिणाम था, जिसमें कई समितियाँ और व्यक्ति इसके मसौदे में शामिल थे।
सीमित भूमिका। अंबेडकर की भूमिका मुख्य रूप से एक रिपोर्टर की थी, जिसे संविधान सभा के निर्णयों को कानूनी भाषा में अनुवादित करने का कार्य सौंपा गया था। वह संविधान के एकमात्र वास्तुकार नहीं थे, और उनके विचारों को अक्सर सभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया गया।
कांग्रेस की उदारता। अंबेडकर की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में स्थिति कांग्रेस नेतृत्व के निर्णय का परिणाम थी कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अपने अतीत के कांग्रेस के विरोध के बावजूद, उन्हें संविधान के मसौदे में एक प्रमुख भूमिका दी गई।
7. आविष्कार, आतंक, हमला: देवत्व की रणनीतियाँ
और, निश्चित रूप से, इन व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की निंदा और अपमान करने का अभ्यास किया है: गांधीजी महान नेता थे, और उससे भी अधिक, वह स्वतंत्रता के लिए उस संघर्ष का महान प्रतीक थे; जैसे अंबेडकर ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर उन्हें कमजोर किया, जैसे कि उन्होंने पच्चीस वर्षों तक महात्मा पर अपमानों की बौछार की, जिन्हें ब्रिटिशों ने इतना मूल्यवान पाया, उनके समर्थक महात्मा को अपमानित और तुच्छ करते हैं।
मौखिक आतंकवाद। अंबेडकर के अनुयायी अक्सर उनके कार्यों या विचारों की किसी भी आलोचना को चुप कराने के लिए मौखिक आतंकवाद और धमकी का सहारा लेते हैं। यह रणनीति असहमति की आवाज़ों को दबाने और अंबेडकर की अपराजेयता के मिथक को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है।
शारीरिक हमला। मौखिक हमलों के अलावा, अंबेडकर के कुछ अनुयायियों ने आलोचकों को चुप कराने के लिए शारीरिक हमलों का सहारा लिया है। यह हिंसा उनके इतिहास के संस्करण को लागू करने और उन लोगों को डराने के लिए उपयोग की जाती है जो उनकी कथा को चुनौती देते हैं।
तथ्यों का दमन। अंबेडकर का देवत्व तथ्यों के दमन की ओर ले गया है जो मिथक के विपरीत हैं। इसमें उनके ब्रिटिशों के साथ सहयोग, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके विरोध, और गांधी की निंदा शामिल है।
8. संविधान का असली लेखन: एक सामूहिक प्रयास
अंबेडकर की रचनाएँ इसी पैटर्न का पालन करती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक अंबेडकर की भाषणों और रचनाओं के चौदह खंड प्रकाशित किए हैं। इनमें 9,996 पृष्ठ शामिल हैं। बारहवें खंड तक के खंड 1946 तक उनके भाषणों और रचनाओं को शामिल करते हैं। इनमें 7,371 पृष्ठ हैं। आपको एक लेख, एक भाषण, एक अंश ढूंढना मुश्किल होगा जिसमें अंबेडकर को भारत की स्वतंत्रता के लिए तर्क करते हुए देखा जा सके। इसके विपरीत।
कई योगदानकर्ता। भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि कई समितियों, उपसमितियों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। यह प्रक्रिया पुनरावृत्त थी, जिसमें मसौदों को फीडबैक और बहस के आधार पर संशोधित और परिवर्तित किया गया।
अतीत का प्रभाव। संविधान ने मौजूदा कानूनी ढांचों पर भारी निर्भरता दिखाई, जिसमें 1935 का भारत सरकार अधिनियम और अन्य देशों के संविधान शामिल थे। यह पूरी तरह से मौलिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि विभिन्न विचारों और अनुभवों का संश्लेषण था।
पुनरावृत्त प्रक्रिया। संविधान चर्चा, बहस और समझौते की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ। विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया गया, और निर्णय अक्सर मतदान के माध्यम से किए गए। अंतिम दस्तावेज़ इस सामूहिक विचार-विमर्श का उत्पाद था।
9. घटनाओं का खींचतान: कैसे इतिहास ने संविधान को आकार दिया
कांग्रेस का संविधान सभा पर पूर्ण नियंत्रण था। 296 सीटों में से, कांग्रेस ने 205 जीतीं। मुस्लिम लीग ने 73 जीतीं। लेकिन बाद में उसने विधानसभा का बहिष्कार किया, स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए एक अलग विधानसभा की मांग की। इसलिए, कांग्रेस के पास 223 सीटों में से 205 थीं।
उथल-पुथल के समय। भारतीय संविधान एक अत्यधिक उथल-पुथल के समय में तैयार किया गया, जिसमें देश का विभाजन, रियासतों का एकीकरण, और गांधी की हत्या शामिल थी। इन घटनाओं ने मसौदा प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाला।
बदलती प्राथमिकताएँ। संविधान सभा का ध्यान विभाजित संघ से एक मजबूत केंद्रीय सरकार की ओर स्थानांतरित हुआ, जो विभाजन की चुनौतियों के जवाब में था। एकता और स्थिरता की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई।
समझौते और समायोजन। संविधान विभिन्न समूहों और दृष्टिकोणों के बीच कई समझौतों और समायोजनों का परिणाम था। कांग्रेस के नेताओं ने विशेष रूप से अपने मतभेदों को भुलाकर एक ऐसा दस्तावेज़ बनाने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार थे जो पूरे राष्ट्र के हितों की सेवा करेगा।
10. दो प्रमुख निर्धारक: शक्ति और पूर्वाग्रह
पिछले पचास वर्षों का कुल परिणाम यह है कि आज फिर से भारत में वही क्रम चल रहा है। लोकमान्य लगभग भुला दिए गए हैं। केरल के बाहर कुछ ही लोग नारायण गुरु को जानते हैं। भक्तों के एक संकीर्ण घेरे के अलावा कोई नहीं जानता कि स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्री ऑरोबिंदो, रामाना महार्षि, कांची के परमाचार्य ने हमें खड़ा करने के लिए क्या किया। स्वामी विवेकानंद को कभी-कभी धूल झाड़कर बाहर लाया जाता है—उसी धर्मनिरपेक्षता के कपड़े पहनाए जाते हैं जिसकी वह निंदा करते। गांधीजी हर दिन अदालत में हैं—एक दिन उन्हें पीछे हटने के लिए, अगले दिन उन्हें मुस्लिम नेताओं को पाकिस्तान पर जोर देने के लिए धकेलने के लिए। और अंबेडकर जैसे व्यक्तियों को देवत्व दिया जाता है।
शक्ति की गतिशीलता। अंबेडकर का देवत्व भारतीय समाज में चल रहे शक्ति संबंधों का परिणाम है। राजनीतिज्ञों ने उनके नाम का उपयोग वोट जुटाने के लिए किया है, और उनके अनुयायियों ने आलोचकों को चुप कराने के लिए धमकी और हिंसा का सहारा लिया है।
पूर्वाग्रह और पूर्वधारणा। अंबेडकर का देवत्व पूर्वाग्रह और पूर्वधारणा से भी प्रेरित है। उनके अनुयायियों ने अक्सर उनके नाम का उपयोग अपने स्वयं के घृणा और अन्य समूहों के प्रति भेदभाव को सही ठहराने के लिए किया है।
देवत्व के परिणाम। अंबेडकर का देवत्व इतिहास की एक विकृत समझ और तथ्यों के दमन की ओर ले गया है। इसने एक भय और आतंक का माहौल भी उत्पन्न किया है जो उनके विरासत पर खुली और ईमानदार चर्चा को रोकता है।
अंतिम अपडेट:
FAQ
What's Worshipping False Gods: Ambedkar and the Facts Which Have Been Erased about?
- Critical Examination of Ambedkar: The book critically analyzes B.R. Ambedkar's life, focusing on his role in the Indian independence movement and his interactions with the British government.
- Historical Context: It places Ambedkar's actions within the broader context of India's struggle for freedom, highlighting his often controversial stance that aligned with British interests.
- Myth vs. Reality: Arun Shourie argues that myths surrounding Ambedkar's legacy have overshadowed the factual history of his political actions and affiliations.
Why should I read Worshipping False Gods by Arun Shourie?
- Understanding Historical Narratives: The book challenges popular narratives about Ambedkar, encouraging readers to think critically about historical figures.
- Insight into Caste Politics: It delves into the complexities of caste politics in India and how Ambedkar's legacy is used in contemporary discourse.
- Engaging Writing Style: Arun Shourie's provocative writing style makes the book both informative and thought-provoking for those interested in history, politics, and social justice.
What are the key takeaways of Worshipping False Gods?
- Ambedkar's Political Stance: The book emphasizes Ambedkar's non-participation in the conventional freedom struggle, often opposing the Congress and supporting British rule.
- Critique of Nationalism: Shourie argues that Ambedkar was critical of nationalism, believing the Congress did not genuinely represent lower caste interests.
- Legacy of Misrepresentation: The author highlights how Ambedkar's legacy has been mythologized, often at the expense of a more accurate understanding of his actions.
What are the best quotes from Worshipping False Gods and what do they mean?
- "Disorientation, and from that disarray...": This quote reflects the author's concern about the consequences of misrepresenting historical figures, suggesting societal fragmentation.
- "The freedom struggle, in his words...": This encapsulates Ambedkar's skepticism towards the nationalist movement, indicating it didn't address lower caste issues.
- "The Congress is deceiving the world...": This critiques the Congress party's use of nationalism, suggesting it masks deeper communal divisions.
How does Arun Shourie portray Ambedkar's role in the independence movement?
- Non-participation in Freedom Struggle: Shourie argues Ambedkar did not engage in the freedom struggle, aligning with British interests for lower caste benefits.
- Criticism of Congress: The book details Ambedkar's consistent criticism of the Congress party, viewing it as serving upper-caste interests.
- Ambedkar's Political Alliances: Shourie highlights Ambedkar's alliances with British officials, suggesting these were more significant than the nationalist movement.
What specific criticisms does Shourie make about Ambedkar's writings?
- Support for British Rule: Shourie points out Ambedkar's belief in British moral responsibility towards Scheduled Castes, undermining the nationalist struggle.
- Allegations Against Congress: The author critiques Ambedkar's claims about Congress's failure to represent lower castes, suggesting exaggeration.
- Historical Revisionism: Shourie contends Ambedkar's writings have been used to distort the historical context of his actions.
How does Worshipping False Gods address the concept of caste in Indian society?
- Caste as a Political Tool: Shourie discusses how caste has been used politically by leaders, including Ambedkar, to mobilize support and create divisions.
- Ambedkar's Vision for Lower Castes: The book explores Ambedkar's vision for upliftment, often relying on British alignment rather than fostering independence.
- Contemporary Relevance: Shourie connects Ambedkar's ideas to current caste politics, suggesting caste continues to shape political discourse.
What is the significance of Ambedkar's relationship with the British government?
- Collaboration with Colonial Powers: Shourie emphasizes Ambedkar's collaboration with the British as a key political strategy for lower caste benefits.
- Critique of Nationalist Leaders: The book argues Ambedkar's relationship with the British was often at odds with nationalist leaders.
- Impact on Historical Memory: Shourie suggests this collaboration has led to a complex legacy for Ambedkar, often misunderstood in contemporary discussions.
How does Worshipping False Gods challenge the popular perception of Ambedkar?
- Myth vs. Reality: The book challenges the mythologized version of Ambedkar as a sole champion of the oppressed, presenting a nuanced view.
- Critique of Deification: Shourie argues against Ambedkar's deification, suggesting it overlooks complexities in his life and work.
- Historical Revisionism: The author calls for reevaluation of Ambedkar's legacy, urging consideration of historical context over simplified narratives.
What are the implications of Shourie's arguments for contemporary Indian politics?
- Caste and Political Identity: Shourie's analysis raises questions about caste's role in contemporary politics, particularly in using Ambedkar's legacy.
- Revisiting Historical Narratives: The book encourages reassessment of historical narratives, crucial for addressing current social issues.
- Impact on Social Justice Movements: Shourie's arguments highlight the need for inclusive understanding of struggles faced by marginalized communities.
How does the book address the evolution of Ambedkar's ideas over time?
- Shift in Political Strategy: Shourie traces Ambedkar's evolving political strategy, noting shifts as he recognized limitations of British collaboration.
- Response to Nationalist Movements: The book discusses Ambedkar's ideas evolving in response to Indian politics, particularly Congress's rise.
- Legacy of Ambedkar's Thought: Understanding Ambedkar's evolving ideas is essential for grasping their relevance in contemporary caste and social justice discussions.
समीक्षाएं
झूठे देवताओं की पूजा की समीक्षाएँ मिश्रित हैं, जो 1 से 5 सितारों तक फैली हुई हैं। समर्थक इस पुस्तक की गहन शोध और अंबेडकर के बारे में लोकप्रिय कथाओं को चुनौती देने के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि आलोचक इसे पक्षपाती और खराब संपादित मानते हैं। कई समीक्षक शौरी के साहस की सराहना करते हैं कि उन्होंने एक विवादास्पद विषय को उठाया, जबकि अन्य उन पर जातिवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। पुस्तक में अंबेडकर की भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका का चित्रण एक प्रमुख विवाद का बिंदु है, जिसमें इसकी सटीकता और निष्पक्षता पर रायें तीव्रता से विभाजित हैं।
Similar Books